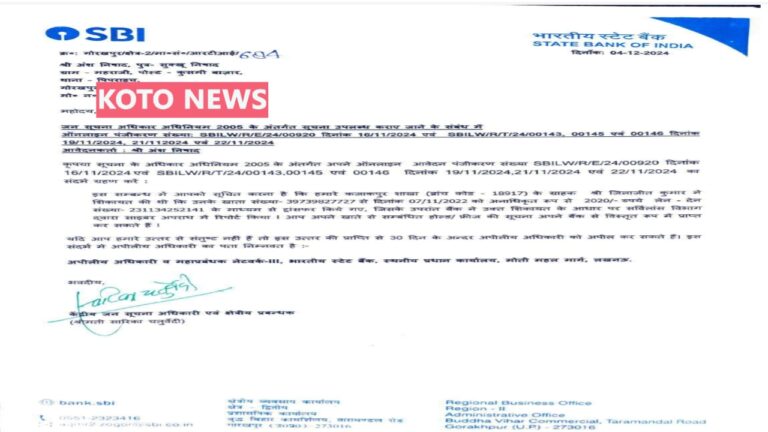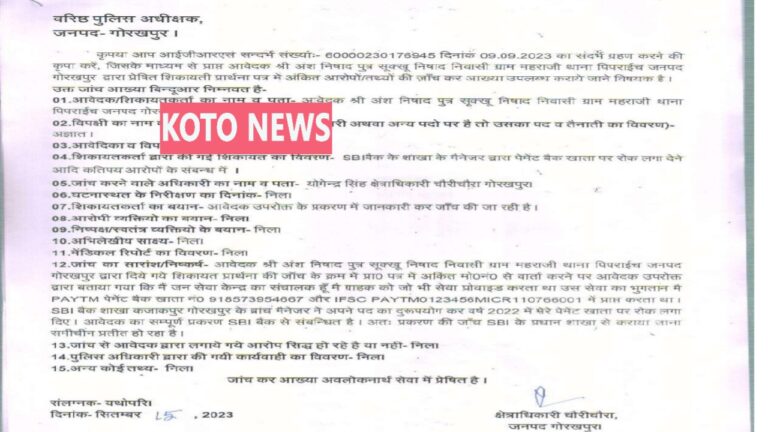एनईएसडीए वे फॉरवर्ड डिजिटल सेवाओं
कोटो न्यूज़ नेटवर्क (KNN) | प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने आरटीएस आयुक्तों के सहयोग से एनईएसडीए वे फॉरवर्ड पहल के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वितरण ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के आरटीएस आयुक्तों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की, जबकि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागड़े भी मौजूद रहे। सेवाओं की उपलब्धता को आसान बना रही है, बल्कि प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का एपीआई लिंकेज आरटीएस आयोगों की वेबसाइटों के साथ अंतिम चरण में है, जिससे राज्य शिकायत अधिकारियों को वास्तविक समय में राज्य-विशिष्ट सेवा शिकायतों का डेटा उपलब्ध हो सकेगा।
सचिव ने स्पष्ट किया कि डीएआरपीजी और आरटीएस आयोग मिलकर भूमि, श्रम, वित्त और पर्यावरण जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में ई-सेवाओं को बढ़ावा देंगे। ये क्षेत्र सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़े हैं और इनके डिजिटलीकरण से ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को भी बढ़ावा मिलेगा। आरटीएस आयोगों से अनुरोध किया गया कि वे अधिसूचित सेवाओं की सूची में इन क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल करने के लिए अपने-अपने राज्यों में पहल करें और राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करें। वर्तमान में देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एनईएसडीए ढांचे के अंतर्गत 22,000 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इन सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव का मूल्यांकन एएकेएलएएन बेंचमार्किंग टूल के माध्यम से किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया है। बैठक में बताया गया कि आरटीएस आयोगों की सर्वोत्तम प्रथाओं को मासिक एनईएसडीए वे फॉरवर्ड रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिससे अन्य राज्य भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने ई-सेवा ढांचे को बेहतर बना सकें।
बैठक में एनसीजीजी के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागड़े ने आरटीएस अधिनियमों के लाभों पर 9 महीनों में किए जाने वाले विस्तृत अध्ययन की जानकारी दी। इस अध्ययन में सार्वजनिक सेवा वितरण और शिकायत निवारण की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। सेवा वितरण के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। डीएआरपीजी ने सभी आरटीएस आयोगों को राज्य सहयोग पहल (SCI) के तहत ऐसे प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया है, जिनसे डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो और नागरिकों को पारदर्शी, कुशल और त्वरित सेवा मिले। यह पहल भारत सरकार की व्यापक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन के परिणामों में सुधार करना है।
फोकस क्षेत्र को विस्तार से समझाते हुए हम कह सकते हैं कि एनईएसडीए वे फॉरवर्ड पहल के तहत चार प्रमुख आयामों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिनका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। ये चारों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर एक ऐसा डिजिटल सेवा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करते हैं जो सभी नागरिकों के लिए उपयोगी और भरोसेमंद हो।
1. डिजिटल सेवाओं की संख्या
इस पहल के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की कुल संख्या का मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि किस राज्य ने कितनी सेवाओं को डिजिटलीकृत किया है और नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। अधिक संख्या में डिजिटल सेवाएं यह दर्शाती हैं कि राज्य प्रशासन ने अपने प्रक्रियाओं को तकनीक के माध्यम से सरल बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, उद्योग, परिवहन, श्रम, वित्त और पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों की सेवाएं शामिल हो सकती हैं। मूल्यांकन से यह भी पता चलता है कि किन क्षेत्रों में अभी भी डिजिटलीकरण की आवश्यकता है और किन राज्यों को इस दिशा में अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है।
2. गुणवत्ता
केवल सेवाओं की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता के आकलन में यह देखा जाता है कि सेवाएं कितनी विश्वसनीय हैं, उनका उपयोग कितना आसान है, और क्या प्रक्रियाएं पारदर्शी हैं। इसमें यूज़र इंटरफ़ेस की सहजता, दस्तावेज़ों की स्पष्टता, और सेवा प्रदान करने में देरी न होने जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाती हैं और भ्रष्टाचार या अनियमितताओं की संभावना को कम करती हैं।गुणवत्ता सुधार के लिए राज्यों को नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी अपग्रेड और उपयोगकर्ता फीडबैक को शामिल करने की सिफारिश की जाती है।
3. उपलब्धता
उपलब्धता का मतलब है कि नागरिकों को सेवाएं आसानी से और जब भी जरूरत हो, उपलब्ध हों। इसका आकलन यह देखने के लिए किया जाता है कि सेवाएं 24×7 उपलब्ध हैं या केवल सीमित समय में। यह भी देखा जाता है कि सेवाएं मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या कियोस्क जैसे विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं। बेहतर उपलब्धता का सीधा असर नागरिकों की सुविधा और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच पर पड़ता है। डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्यों को बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर क्षमता, और बैकअप सिस्टम पर निवेश करना पड़ता है ताकि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण सेवाएं बाधित न हों।
4. नागरिक संतुष्टि
अंततः किसी भी सेवा का असली मूल्य उस सेवा का उपयोग करने वाले नागरिक ही तय करते हैं। नागरिक संतुष्टि का आकलन नागरिकों के अनुभव, सेवा प्राप्त करने की सरलता, और शिकायत निवारण की प्रभावशीलता के आधार पर किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि शिकायत दर्ज करने और उसे सुलझाने की प्रक्रिया कितनी तेज और पारदर्शी है। नागरिकों से नियमित रूप से फीडबैक लेकर सेवाओं में सुधार करना इस क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। उच्च नागरिक संतुष्टि न केवल सरकार की छवि को मजबूत करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल इंडिया का विज़न जमीनी स्तर पर साकार हो रहा है।
उपकरण और तकनीकी सहयोग
एनईएसडीए वे फॉरवर्ड के मूल्यांकन कार्य में एएकेएलएएन (AeklaAn) बेंचमार्किंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने विकसित किया है। यह टूल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की डिजिटल सेवाओं को विभिन्न मानकों पर परखता है, जैसे:सेवा तक पहुँचने में लगने वाला समय वेबसाइट/पोर्टल की उपयोगकर्ता-मित्रता मोबाइल व वेब एप्लिकेशन की कार्यक्षमता नागरिक प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण दर
लक्ष्य
सभी नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक अधिकारों को मजबूत करना। राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना और अपनाना। डिजिटल इंडिया के विज़न को ज़मीनी स्तर पर लागू करना।
आरटीएस आयोगों की भूमिका
आरटीएस (Right to Service) आयोग एनईएसडीए वे फॉरवर्ड के कार्यान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
उनकी प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं: सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों को तय समय सीमा के भीतर सेवा मिले। शिकायतों का निवारण: सेवा में देरी, अनियमितता या असंतोष की स्थिति में समय पर समाधान। ई-सेवाओं का विस्तार: भूमि, श्रम, वित्त और पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना। सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना: सफल मॉडलों और रणनीतियों को अन्य राज्यों के साथ साझा करना। API लिंकिंग और डेटा मॉनिटरिंग: सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल को आरटीएस आयोग की वेबसाइटों से जोड़कर वास्तविक समय में डेटा साझा करना।
Source : PIB | रिपोर्ट : कोटो न्यूज़ नेटवर्क (KNN) |